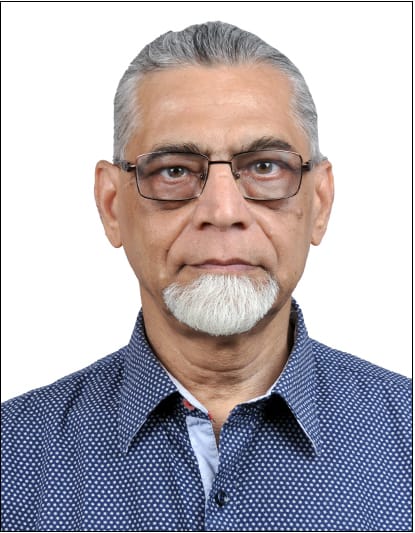धर्म
धर्म
धर्म की सार्वभौमिक परिभाषा है, धारयते इति धर्मः,जिसे धारण किया जाय, वह धर्म। यह धर्म शब्द मूलरूप से “धृ” धातु से लिया गया है और उसका “म” से संयोजन करके कह दिया, धर्म। “धृ” का मुख्य अर्थ है, धारण करना। मूलरूप से जीवनी अस्तित्व का आधार धर्म है। ऐसे अस्तित्व से जो जुड़ा है, वह है “म”, मकार। इस उक्ति से “म” को धारण करना ही धर्म है।
मकारेण उच्यते ब्रह्म मकारेण नन्द नन्दनः।
मकारेण कामदेवो इति मकारेण मुक्ति बन्धनः।
“म” के दो मूल अर्थ हैं। पहला आनन्द और दूसरा वासना। इनमें से जिसे धारण किया जाता है, वही धर्म हो जाता है। एक धर्म वह जो बांधता है और एक धर्म वह जो मुक्त करता है। दोनों अवस्थाओं में कहलाता वह धर्म ही है। यदि आनन्द को चुना तो मुक्ति और वासना को चुना तो बन्धन। मजेदार बात यह है कि आनन्द का द्वार वासना के भीतर से ही निकलता है। वासनाजन्य बन्धन को गहरे में जाने बिना मुक्ति का द्वार नहीं खुलता। धर्म के अदृश्य गुण को जानना है तो वासनारूपी जंगल के भीतर से गुजरना ही होगा, उसकी पगडंडियों पर चलना ही होगा। ये पगडंडियां अदृश्य हैं। इन्हें समझना है तो हमें रघुवंशम् में दिए कालिदास द्वारा विरचित एक सूत्र के अन्तर्भेद के रहस्य को जानना होगा। वह सूत्र है, षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एषः।
इस सूत्र का अनावरण करने से पूर्व मैं संस्कृत भाषा के प्रबुद्ध मनीषियों से क्षमायाचना करना चाहूंगा क्योंकि इस सूत्र का जो भेद प्रकट करने जा रहा हूं, वह कालिदास द्वारा कहे सूत्र के अर्थ से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। इसलिए क्षमायाचना।
षष्ठांशवृत्तेरपि, मन की छः वृत्तियां हैं… काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये सभी षष्ठांशरूप में मन में व्याप्त वासना के एक बटे छः अंश हैं। मन इनका सम्राट है। ये ऐसे हुए, जैसे राजा के भृत्य। पूर्वकाल में जिस प्रकार राजा कर के रूप में प्रजाजनों से उनकी आय का षष्ठांश बसूलता था, उसी प्रकार मन भी इन वृत्तियों द्वारा कर के रूप में मनुष्य से उसका सुख बसूलता है। अब जबरन धन बसूला जाए या सुख, दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य दुख का अनुभव करता है। दुख अर्थात सुख का विलोपन। मन की छः भर्त्यरूपी वृत्तियां और सभी के दायरे में एक बटा छः सुख बसूलने का दायित्व, अर्थात मन द्वारा तुमसे पूरा का पूरा सुख छीनने का षड्यन्त्र। यही कारण है कि मन के सक्रिय रहते मनुष्य कभी सुखी नहीं रह पाता। यहां मन की रघुवंशम् के राजा से कोई तुलना नहीं है। यहां मन एक प्रकार का डाकू है, जैसेकि आज के युग के राजा हैं। जिस प्रकार राजा के भृत्य छल-बल का प्रयोग करके प्रजा का धन लूटते हैं, वैसे ही मन छल से भरी वृत्तियों का प्रयोग करके मनुष्य का सुख लूटता है। उनका धर्म मकारेण कामदेवो इति का प्रतिरूप होता है। जब किसी के पास प्रचुर धन आने लगता है तो सबसे पहले उसके ऊपर दो लोगों की नज़र पड़ती है, डाकू और राजा। आज का राजा राजा कम है, डाकू ज़्यादा है और डाकू का एक ही काम है, लूटना। मन भी यही करता है। वह तुम्हारे भीतर मरूपी कामवासना जगाकर सांसारिक धन-सम्पत्ति का अनावश्यक संचय करने के लिए प्रेरित करता है। यदि तुम कामरूपी मतत्त्व को धारणकर लोगे तो कामना ही तुम्हारा धर्म बन जायगा। कामना के धर्म बनते ही मन में इच्छाओं का ज्वार उठता है। फिर इस ज्वार के उठते ही कामवासना का भंवर तुम्हें अपने में चपेट लेता है और तुम उसमें डूबते जाते हो।
आज के युग में इच्छा ही मनुष्य का धर्म हो गया है। वह इच्छाओं का गुलाम बन गया है। उसने वासना के बहुवर्णी वस्त्र धारण कर लिए हैं। वासना/कामना/इच्छा अर्थात बन्धन। मनुष्य को इच्छाओं में बंधना अच्छा लगता है, इसलिए उसने नाना प्रकार के धर्म खड़े कर लिए हैं। फिर जितना बड़ा धर्म, उतनी ही अधिक इच्छाएं और उतने अधिक बन्धन। जैसे बंधना ही धर्म हो।
धारयते इति धर्मः,जिसने धर्म की यह परिभाषा की होगी, वह प्रबुद्ध व्यक्ति रहा होगा। इसलिए कहता हूं कि मतत्त्व के रूप में धर्म बांधता भी है, बन्धनः। बन्धन विकृति है। इससे मुक्त होना है तो मन के म को अप्रकट होना होगा। म के विलुप्त होते ही न शेष रह जायगा। संस्कृत शब्दकोश में न का अर्थ है, खाली हो जाना। तुम हर प्रकार की वासना/कामना/*इच्छा से खाली हुए। खाली अर्थात शून्य, इस शून्य में ही ब्रह्म उतरता है। ब्रह्म यद्वा मतत्त्व को “ब्रह्” यद्वा सुकृतस्वरूप में ओढ़े हुए।
मन अर्थात विचारों की भीड़, वासना अर्थात इच्छाओं की भीड़। मन के जगत में भीड़ का होना ही धर्म है। भीड़ अर्थात दूसरों की ओर ध्यान, स्वयं पर कोई ध्यान नहीं। यहां स्वतत्त्व बिसर जाता है और परतत्त्व में रम जाना ही मंत्र बन जाता है। पर का जगत बाहर का जगत है और बाहर के जगत में विचार हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं। वहां तुम खाली नहीं हो सकते, और जब तक इनसे खाली नहीं हो जाते, अपने स्वतत्त्व के प्रति जागरूक नहीं हो सकते।
इस तरह धर्म के दो स्वरूप हुए, विकृत और सुकृत। जब वह विकृत होगा तो भीतर वासना का साम्राज्य होगा और चित्त में विकारों की भीड़ होगी। जब वह सुकृत होगा तो चित्त वासनाशून्य हो जाएगा। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि क्या धारण करते हो।
ब्रह्म एक है, आनन्द एकाकी है और स्वतत्त्व एकान्तित है। इस उक्ति से ब्रह्म, आनन्द और स्वतत्त्व पर्यायवाची शब्द हुए। वे भीड़ में नहीं मिलते। भीड़ का अर्थ है शोरगुल, अशान्ति, अव्यवस्था। ब्रह्मसूत्र कहता है कि भीड़ का जमावड़ा होते ही वे अदृश्य हो जाते हैं, “अदृश्यत्वादिगुणको”। धर्म के गुण या रहस्य एकान्त में ही प्रकट होते हैं। एकान्त का अर्थ है, अन्त में केवल एक बचे। इसे ही कृष्ण ने स्वधर्म कहा है। वे कहते हैं कि भीतर छिपे स्वतत्त्व को जानो और उसे धारणकर लो। भीतर एकान्त है, परम शान्ति है। वहां कोई शोरगुल नहीं है, न विचारों का, न इच्छाओं का। जब सारे शोर मिट जाते हैं, तभी एकान्त का संगीत प्रकट होता है। यदि इस संगीत को हृदयपटल पर धारण करके संगीतमय हो जाओ तो भीतर जिस नन्द-नन्दन की अनुभूति होती है, वह जैसे जीवन का मंत्र बन जाता है। इसका अर्थ हुआ कि आनन्दरूपी मत्त्व को धारण करना ही सच्चा धर्म है, अन्य धर्म तो छद्म हैं, झूठे हैं।
लेखक- मदन गोपाल गुप्ता “अकिंचन”
कानपुर उत्तर प्रदेश